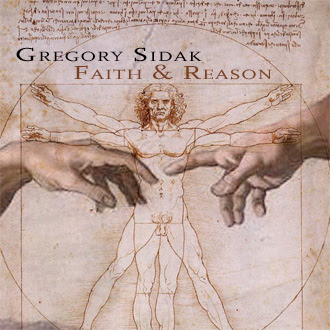आस्था के लिए व्यक्ति का पहले से ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है और न ही उसमें तर्कशक्ति होने आवश्यकता होती है. आस्थावान को तो बस किसी दूसरे व्यक्ति से जानना और मानना होता है, इसमें न तो बुद्धि की आवश्यकता होती है और न ही किसी श्रम की. अतः यह अतीव सरल है, इसलिए आस्था निष्कर्म्य लोगों के लिए एक बड़ा शरणगाह है - बिना कोई प्रयास किये उनकी जिज्ञासा संतुष्ट हो जाती है. जिज्ञासा संतुष्ट होने पर व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी कह सकता है किन्तु उसका सभी ज्ञान उथला होता है और जो प्रायः समयानुसार तथा परिपेक्ष्यानुसार परिवर्तित होता रहता है. मान लीजिये कि एक व्यक्ति आस्तिकों के समूह में जाता है और उनकी बातें सुनकर आस्तिक हो जाता है. वही व्यक्ति जब नास्तिकों के समूह में जाता है तो उनकी बातें सुनकर बड़ी सरलता से नास्तिक हो सकता है. इस प्रकार उसकी आस्था और ज्ञान परिवर्तनीय होते है. अपनी आस्था को स्थिर रखने के लिए वह बहुमत का आश्रय लेता है अर्थात जिस बात को अधिक लोग कहते हैं वह उसी में आस्था रखने लगता है.
इसके विपरीत, विवेक पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना एक क्लिष्ट, श्रमसाध्य एवं बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति प्रत्येक तथ्य का तर्क की कसौटी पर परीक्षण करता है और संतुष्ट होने पर ही उसे स्वीकार करता है. इस प्रक्रिया में व्यक्ति में तर्कशक्ति के अतिरिक्त कसौटी पर परीक्षण का पूर्व ज्ञान भी होना भी अपेक्षित है. अतः ज्ञानवान व्यक्ति ही विवेकशील हो सकता है. चूंकि यह वैज्ञानिक प्रक्रिया क्लिष्ट है इसलिए व्यक्ति सीमित ज्ञान ही प्राप्त कर पाता है किन्तु उसका ज्ञान गहन और अपरिवर्तनीय होता है. सीमित ज्ञान होने के कारण ऐसा व्यक्ति सदैव जिज्ञासु बना रहता है और वह स्वयं को सदैव अल्पज्ञानी ही मानता है. इसी भावना के कारण वह अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि के प्रयास करता रहता है. वस्तुतः यही मनुष्यता है जो मनुष्य की अंतर्चेतना जिज्ञासा को जीवंत बनाए रखती है.
आस्था मनुष्य का प्राकृत गुण नहीं है, इसे मनुष्य जाति ने केवल अंतरिम रूप में काम चलाने हेतु अपनाया था. जब मनुष्य के पास ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत सीमित थे और वे उसकी जिज्ञासा को तृप्त करने हेतु अपर्याप्त थे, उसका विवेक भी अपर्याप्त था. अतः उसने अपनी जिज्ञासा को तात्कालिक रूप से तृप्त करने के लिए आस्था का आश्रय लिया, किन्तु यह स्थायी हल नहीं है. विज्ञानं ही मनुष्य जाति की अंतर्चेतना जिज्ञासा को तृप्त करने का स्थायी हल है.

मनुष्यता में भी निर्जीव वस्तुओं की तरह कुछ जड़ता होती है जो उसे निश्कर्मी बने रहने की सुविधा प्रदान करती है. अतः सुविध्वादी मनुष्य आज भी आस्था का दामन कस कर पकडे हुए हैं ताकि वे विज्ञानं की श्रमसाध्य एवं क्लिष्ट प्रक्रिया से बचे रह सकें.